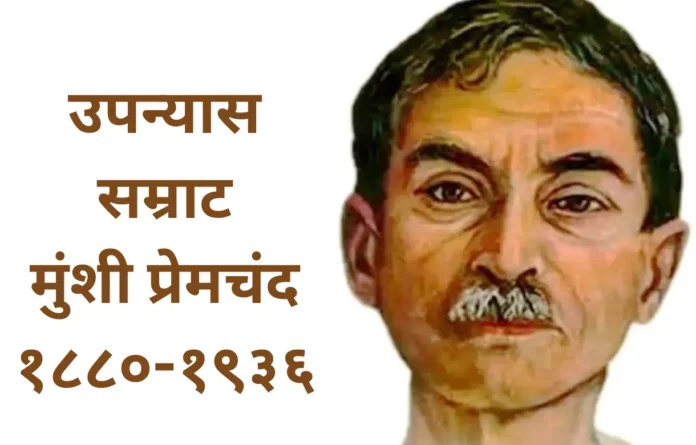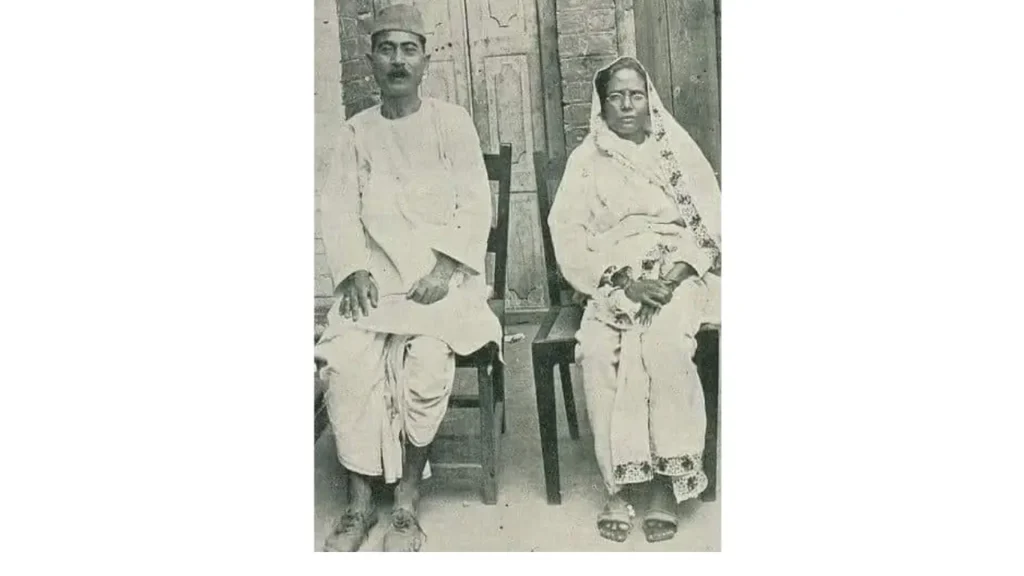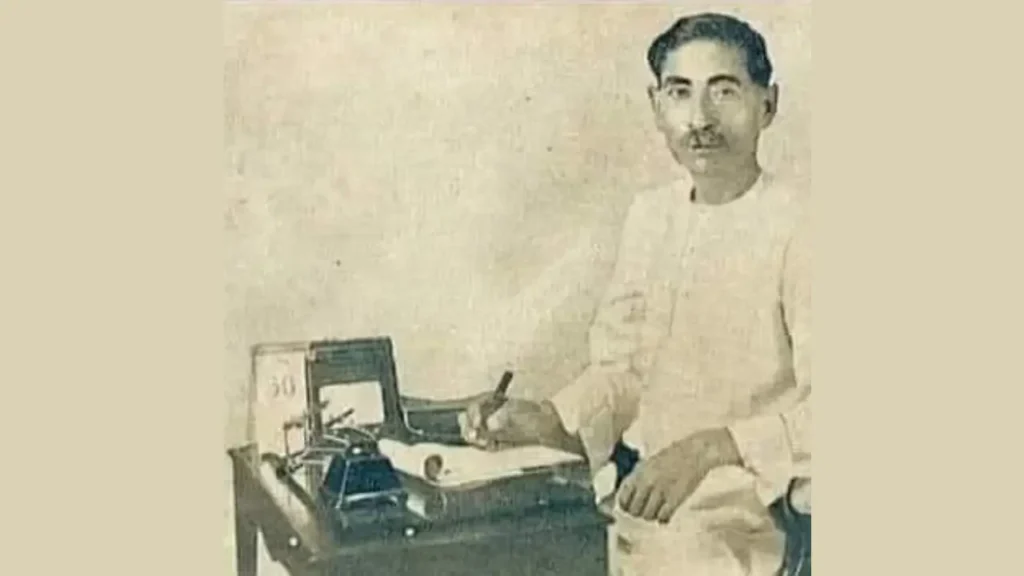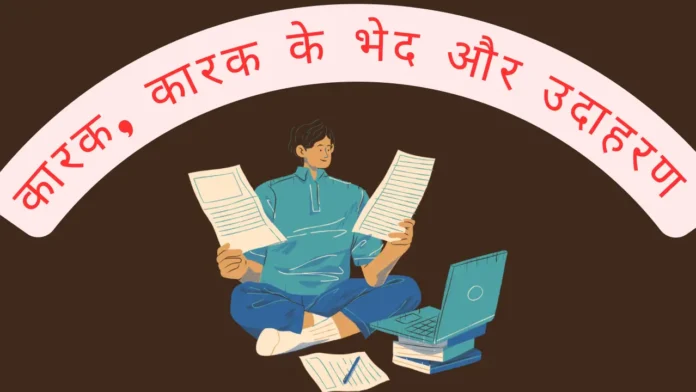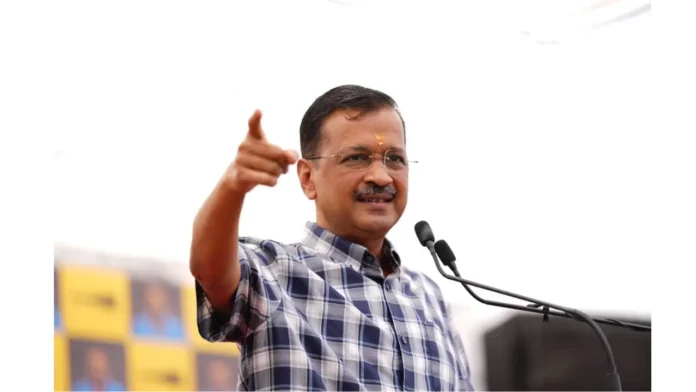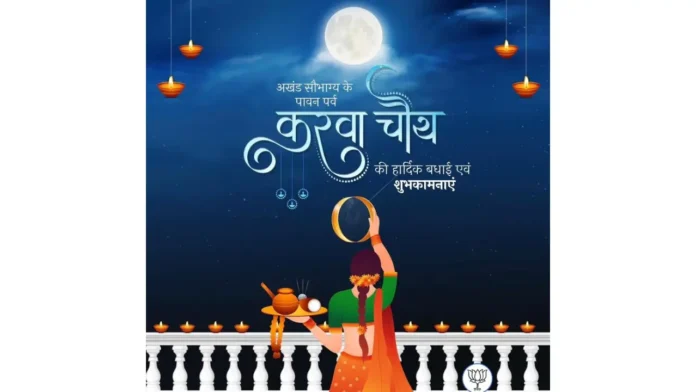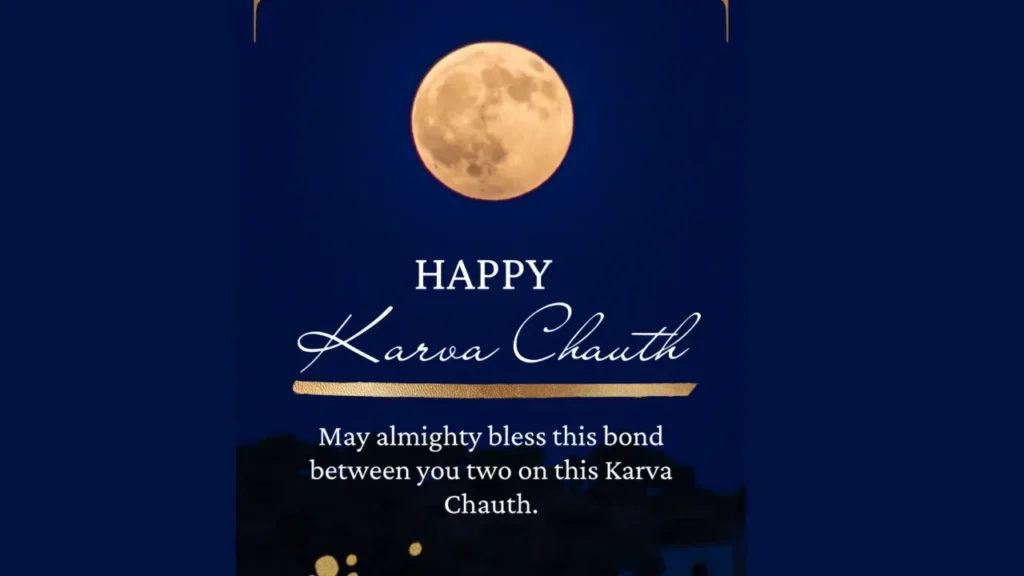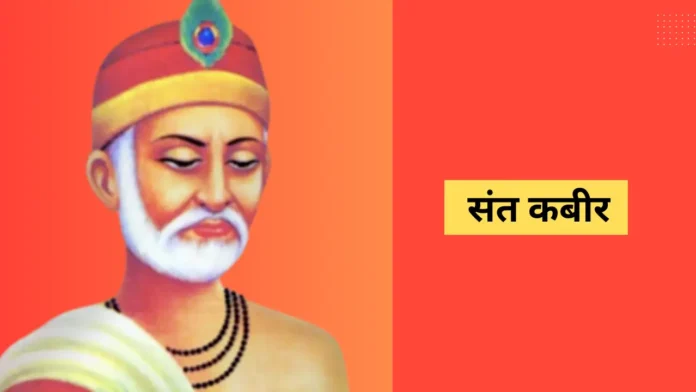बक़रीद 2025- बक़रीद एक अंतरराष्ट्रीय त्योहार है। यह ईद उल फित्तर के 70 दिन बाद मनाया जाता है। इस त्योहार को बकरीद जिसे ईद-उल-अजहा तथा ईद-उल-जुहा के नाम से भी जाना जाता है।
बकरीद का त्योहार बकरे की क़ुर्बानी का प्रतीक माना जाता है तथा यह त्योहार इस्लामी चंद्र कैलेंडर के बारहवें महीने में मनाया जाता है। इस साल बकरीद का त्योहार 17 जून, 2024 को मानाया जाएगा तथा इस पावन दिन पर लोग हज जैसी पवित्र दरगाह की यात्रा करते है।
बक़रीद का अर्थ (Bakrid meaning in hindi)
बक़रीद का अर्थ क़ुर्बानी वाली ईद से लिया जाता है। यह त्योहार क़ुर्बानी का त्योहार है। इसे ईद उल ज़ुहा, ईद अल-अधा, ईद अल-अज़हा, बक़्रईद, बक़्रीद, क़ुरबानी की ईद, इदे क़ुरबाँ आदि कई नामों से जाना जाता है। पवित्र त्योहार रमजान के 70 दिन बाद बक़रीद का त्योहार आता है। बक़रीद साल के अंतिम माह भी होता है। आम धारणा यह है कि बक़र का अर्थ, बकरे से लिया जाता है। इसी नाम से बक़रीद, या बक़्रईद, बक़्रीद प्रसिद्ध होने लगा।
बक़रीद 2025: बक़रीद कब है 2025 (Bakrid 2025 Date)
वर्ष 2025 में बकरीद का त्योहार 7 जून, दिन- शनिवार को मनाए जाने की उम्मीद है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बकरीद का त्योहार त्याग, आत्मसमर्पण तथा आस्था का प्रतीक है। बकरीद को क़ुर्बानी वाली ईद भी कहा जाता है। यह त्योहार रमजान के 70 दिन बाद मनाया जाता है, इस्लाम धर्म में ईद के बाद दूसरा बड़ा त्योहार बकरीद को ही माना जाता है।
| 2025 | 7 जून, दिन- शनिवार |
बक़रीद का इतिहास : बक़रीद क्यों मनाया जाता है ? (Why is Bakrid celebrated?)
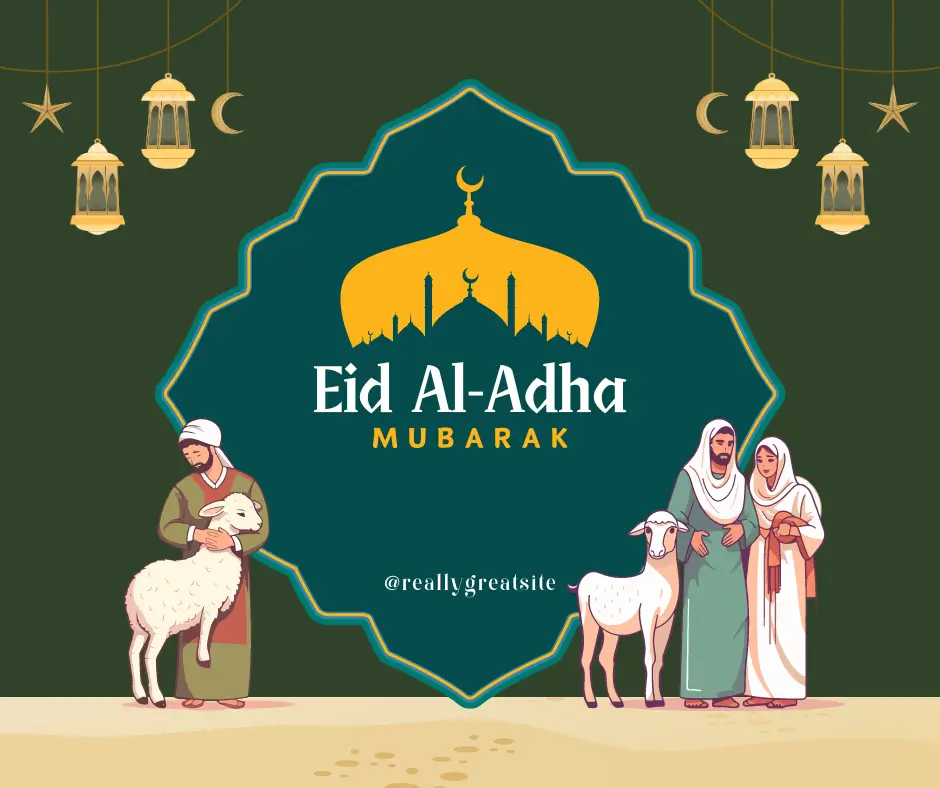
बकरीद का त्योहार मनाने के पीछे हज़रत इब्राहिम से जुड़ी एक रोमांचक घटना है जो इस प्रकार है, हज़रत इब्राहिम जो अल्लाह के के प्रति असीम आस्था रखते थे एवं वे हर रोज़ अल्लाह की इबादत किया करते थे। हज़रत इब्राहिम के परिवार में उसकी पत्नी एवं एक पुत्र था, पुत्र का नाम इस्माइल था। एक दिन इब्राहिम के सपने में अल्लाह आते है और इब्राहिम की परीक्षा लेते हुए यह कहते है कि अल्लाह के प्रति तुम्हें अपनी भक्ति, निष्ठा एवं आत्मसमर्पण सिद्ध करना होगा। इसके लिए अपनी किसी प्रिय तथा क़ीमती चीज़ की क़ुर्बानी देनी होगी, तो इस बात को लेकर इब्राहिम काफ़ी सोच में पड़ जाता है।
हज़रत इब्राहिम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने बेटे इस्माइल से प्यार करता था तथा वह अपने दिल पर पत्थर रख कर अपने बेटे की क़ुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है।
क़ुर्बानी के दौरान इब्राहिम अपनी आँखो में पट्टी बांध लेते है ताकि वह अपने बेटे का चेहरा न देख सके और जैसे ही ये अपने बेटे की क़ुर्बानी देने जाते है तो बेटे के जगह एक बकरे की क़ुर्बानी हो जाती है और इस्माइल बच जाता है। अल्लाह हज़रत इब्राहिम की यह निष्ठा देख कर काफी प्रसन्न होते है और इस घटना के बाद से बक़रीद के दिन बकरा की क़ुर्बानी देने की चलन शुरू हो गई।
बक़रीद का बकरा (Bakrid ka bakra)

बक़रीद का बकरा त्याग, भक्ति, निष्ठा एवं आत्मसमर्पण और आस्था का प्रतीक है। यह पैगंबर इब्राहिम (अब्राहम) द्वारा परम शक्ति एवं संसार के रचियता अल्लाह के आदेश पर अपने बेटे की बलि देने के लिए आतुर हो जाने की भावना को व्यक्त कराता है। बक़रीद के बकरे का गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस उत्सव का केंद्र ही बलि का बकरा है।
इस प्रकार बकरीद के दौरान बकरे की बलि देने की प्रथा की शुरुआत हो जाती है।
बक़रीद के बकरे का चुनाव कैसे किया जाता है?
बकरीद के लिए बकरे का चयन धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि बकरा स्वस्थ होना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए और बकरे की आयु एक वर्ष या उससे अधिक की नहीं होनी चाहिए। त्यौहार से कुछ दिन पहले लोग सबसे अच्छा बकरा ख़रीदने के लिए बाज़ार जाते हैं। चुने गए बकरे की तब तक ध्यान रखा जाता है, जब तक बलि नहीं दी जाती।
बकरीद के दिन मस्जिद में विशेष नमाज़ के बाद बलि की रस्म शुरू होती है। बलि दिए गए बकरे के मांस को तीन भागों में बांटा जाता है: एक परिवार के लिए, एक रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, और एक भाग ग़रीबों के लिए।
बक़रीद का चाँद (Bakrid ka Chand) का महत्व
आप सभी ने हिजरी कैलेंडर का नाम सुना होगा, यह इस्लाम धर्म का प्रमुख कैलेंडर है। इसे चंद्र कैलेंडर भी कहा जाता है। इस चंद्रा कैलेंडर में 12 माह होते हैं एवं कुल दिनों की संख्या 354 या 355 होते हैं। हिजरी कैलेंडर चंद्रमा के चक्रों पर निर्भर करता है। प्रत्येक महीने की शुरुआत नए चाँद के दिखने से होती है। त्योहारों की तिथि की घोषणा नए चाँद के दिखने पर निर्भर करता है। बकरीद की तारीख हर साल बदलती रहती है, क्योंकि यह चंद्र चक्र पर निर्भर करती है।
बकरीद चाँद का ख़ास महत्व है क्योंकि यह ईद-उल-अज़हा के आगमन का प्रतीक है। बक़रीद का चाँद इस्लामी कैलेंडर के 12वें और अंतिम महीने धू अल-हिज्जा के 10वें दिन दिखाई देने का संकेत देता है, इस दिन ईद-उल-अज़हा मनाई जाती है। यह त्योहार खुशी, एकता, भाईचारे एवं सामूदायिक की भावना का प्रतीक है। इस दिन दुनिया भर के लोग, चाहे वे किसी भी देश या स्थान पर हों, एक ही चाँद को देखते हैं, जिससे वैश्विक एकजुटता की भावना को बढ़ावा मिलता है।
बक़रीद का रोजा कब है? (Bakrid ka roza kab hai)
यों तो रमजान का रोजा सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण रोजा है। पर बकरीद का रोज़ा का खास महत्व है। कहा जाता है कि बक़्रिद का रोजा नेकी को बढ़वा देता है। यह वर्ष का अंतिम माह होता है। इस त्योहार के शुरू होने से पहले 9 दिन तक रोजा रखे जाते हैं। बकरीद से पहले का दिन, जिसे अराफा का दिन कहा जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह इस्लामी महीने जिल-हिज्जा का 9वाँ दिन होता है।
अराफा के दिन उपवास करना अत्यधिक अनुशंसित है। ऐसा माना जाता है कि यह पिछले वर्ष और आने वाले वर्ष के पापों के प्रायश्चित से मुक्ति दिलाता है। 10वें दिन बक़रीद मनाया जाता है और इस दिन रोजा नहीं रखा जाता है।
बक़रीद का त्योहार कैसे मनाया जाता है?
बकरीद का त्योहार आने से पहले लोग इसकी तैयारी में जुट जाते है तथा 10 दिन पहले ही लोग अपनी घर की साफ-सफाई करने लगते है तथा अन्य त्योहारों की तरह लोग बकरीद में पहनने के लिए नये कपड़े ख़रीदते है तथा इस दिन लोग अपने मित्रों को घर पर इन्वाइट करते है और इस खास अवसर पर तरह-तरह के पकवान बनाए जाते है।
नए कपड़े पहनना, विशेष प्रार्थना करना और दोस्तों और परिवार से मिलना आम रीति-रिवाज हैं। इस दौरान गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान देने जैसे महान कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। बकरीद के दिन बकरे की क़ुर्बानी दी जाती है और इस पावन दिन पर कई जगहों में जरूरत मंदो को भोजन कराया जाता है।
बक़रीद का महत्व:
मुस्लिम समुदाय में बकरीद के त्योहार का विशेष महत्व है। इस दिन दुनिया भर के मुसलमान बकरीद के चांद को देखते हुए, एक-दूसरे से जुड़ते हैं, बलिदान एवं ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखकर इस त्योहार को बड़े ही धूम-धाम से मानते हैं।
बकरीद का यह त्योहार भाईचारे का प्रतीक है। तथा इस दिन लोग अल्लाह को याद कर नमाज अदा करते है और लोग एक-दूसरे से गले मिलकर बकरीद के त्योहार का बधाई देते है और मिठाइयाँ बाँटते है।
बकरीद के उत्सव का आर्थिक महत्व भी है। बलि अर्थात् फ़र्ज़ ए क़ुर्बानी के बकरे की माँग बाज़ार में सबसे अधिक होती है। इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
बक़रीद आस्था, बलिदान, धर्मार्थ कार्यों और सामुदायिक भावना को भी व्यक्त करता है। इस दिन लोग ग़रीबों एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मदद करते हैं। क़ुर्बानी के मांस का एक हिस्सा उन्हें भी दिया जाता है।
यह भी पढ़े:
1-फिल्मी सुपर स्टार कार्तिक आर्यन की फिल्में, जीवन परिचय, उम्र, हाइट, नेट वर्थ आदि सब कुछ।
2 –Khesari Lal Yadav : खेसारी लाल यादव की जीवनी, फिल्में, नेटवर्थ, उम्र एवं परिवार के बारे में।